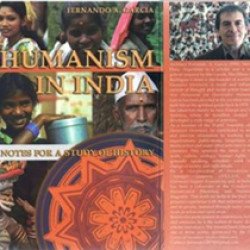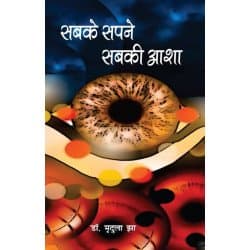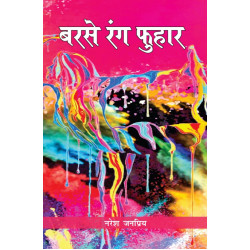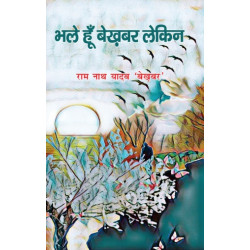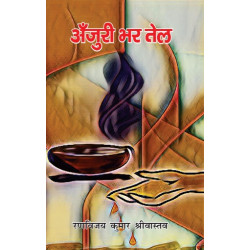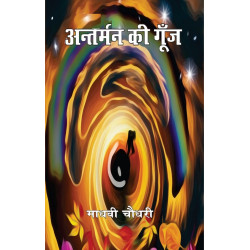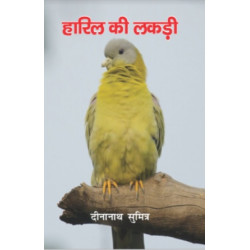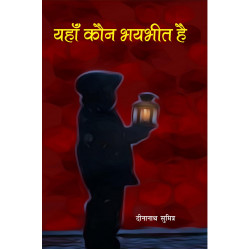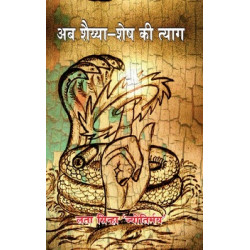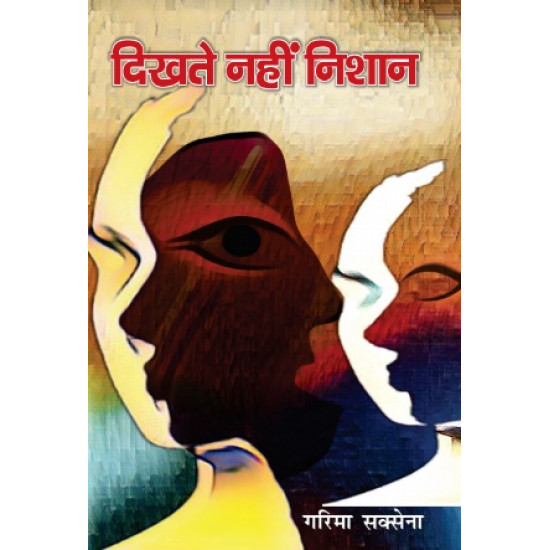
दिखते नहीं निशान
गरिमा सक्सेना
ISBN: 978-93-88946-54-4
पुस्तक समीक्षा : दिखते नहीं निशान
कवयित्री : Garima Saxena
समीक्षक : राहुल शिवाय
प्रकाशक : Best Book Buddies
प्रकाशन वर्ष : 2019
गरिमा सक्सेना हिन्दी गीत, नवगीत, छंद कविताओं की नवीनतम पीढ़ी की रचनाकार हैं। पिछले कुछ एक वर्षों में हिन्दी की लघु पत्रिकाओं में सर्वाधिक छपने वाली रचनाकार भी कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मुझे इनकी साहित्यिक यात्रा को देखकर वर्षों पूर्व आचार्य जानकी बल्लभ शास्त्री जी की कही एक बात याद आती है "पहले पचास-सौ पत्रिकाओं में छपिये। अपनी रचनाओं से अपनी पहचान बनाइये। फिर पुस्तक का विचार कीजिये।"
'दिखते नहीं निशान' गरिमा जी का प्रथम काव्य-संग्रह है जिसमें 29 विषयों पर इनके विभिन्न दोहे संकलित हैं। ये दोहे इनकी कारयित्री प्रतिभा की अभिनवता, व्युतपत्ति की विशदता और अभ्यास की उत्कट अभिप्सा प्रतिलक्षित करती है। इसमें इनका संस्कार उसी प्रकार प्रतिलक्षित होता है जैसे जल पर तेल। मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि जहाँ आज अधिकतर दोहा-संग्रह शिल्प और भाषा की अनेक ग़लतियों के साथ मन को खिन्न करते हैं वहीं इनके संग्रह में शिल्प की सुगढ़ता मन को प्रसन्न करने वाली है। तुकांत, लय, समन्वय आदि का जिस प्रकार गहराई से ध्यान रखा गया है वह निश्चय ही प्रशंसनीय है। इन्होंने दोहा लेखन में जो श्रम किया है वह अपने इस दोहे के माध्यम से बताती भी हैं-
मथा विचारों का दही, ले मथनी जब मीत।
निकला तब अनमोल-सा, दोहा बन नवनीत।।
मानव एक संवेदनशील एवं विवेकशील प्राणी है। उसकी इस संवेदना एवं विवेक की उदात्तता-अनुदत्तता को जब स्वरूप प्राप्त होता है तो वह कला बनकर प्रस्तुत होती है। इन कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला साहित्य है। और इस कारण ही साहित्य मनुष्य के अन्त: जीवन का सौंदर्यशास्त्र भी है। प्रगतिवादी सोच, जीवन मूल्य और कर्तव्य साहित्य को भले ही समकाल से जोड़ते हैं पर इसकी अति साहित्य के निजी तत्व और मानवीय संवेदनाओं को समाप्त भी कर देते हैं.. और साहित्य सिर्फ़ विरोध का माध्यम बनकर रह जाता है। गरिमा जी इस बात को बख़ूबी समझती हैं। उन्होंने अपने दोहों में जहाँ समकाल के अनिवार्य विषयों को छुआ है वहीं प्रेम, संबंध, त्योहार और नीति की सुखद व्याख्या भी की है। और यह विविधता ही उन्हें सामयिकता के साथ कालजयी आयाम भी प्रदान करती है। उदाहरण स्वरूप माँ, पिता, बेटी, प्रेमिका आदि संबंधों पर लिखे उनके दोहे द्रष्टव्य हैं-
सदा सुधा ही बाँटती, सहती शिशु की लात।
माँ आँचल में प्रेम भर, सिंचित करती गात।।
पुनः पिताजी त्यागकर, अपना प्रिय सामान।
ले आये बाज़ार से, बच्चों की मुस्कान।।
बेटी हरसिंगार है, बेटी लाल गुलाब।
बेटी पूरे कर रही, दो-दो घर के ख़्वाब।।
लगीं शिरायें काँपने, बजने लगे सितार।
अनजानी छवि से मिला, जब अनबोला प्यार।।
मेरे जीवन वृत्त का, केंद्र-बिंदु हैं आप।
श्वासों के परिमाप पर, करूँ आपका जाप।।
जैसा कि मैंने पूर्व में कहा है, गरिमा जी के दोहों में विषयों की विविधता उन्हें विस्तृत आयाम प्रदान करती है। इनमें विसंगतिपरक सम्प्रति यथार्थ, जीवन-मूल्यों की गिरावट, राजनीतिक क्षरण आदि पर गहरा असंतोष व्यक्त किया गया है। हो भी क्यों न? जो कविता मानव की मूलभूत भावना का सम्मान करते हुए, एक उपेक्षित उत्तुंगता का संस्पर्श रखवाने का सामर्थ्य रखता हो, वह मानव के भावनात्मक सौंदर्य के साथ-साथ संघर्ष और सामाजिक यथार्थ को भी अवश्य अभिव्यक्ति प्रदान करेगा। यथा-
भूख, गरीबी, आपदा, व्यापारी, सरकार।,
एक कृषक की मौत के, कितने ज़िम्मेदार।।
बदहाली की ज़िंदगी, शोषण, पीर, अभाव।
कृषकजनों की देह पर, रोज़ बो रहे घाव।।
भारत माँ का ताज है, गरिमा है कश्मीर।
आह! मगर यह हो गया, नफ़रत की प्राचीर।।
धूप ओढ़कर दिन कटे, शीत बिछाकर रात।
अच्छे दिन देकर गये, इतनी ही सौगात।।
नारे, भाषण, चुटकुले, जुमले, भ्रष्ट-बयान।
राजनीति की किस तरह, बदल गयी पहचान।।
जिन्हें सलामी दे रहा, नित्य इंडिया गेट।
उन्हीं शहीदों के स्वजन, सोते भूखे पेट।।
रोज़ डिग्रियों से करे, भूखा युवक सवाल।
क्यों न मुझे तुम दे सकीं, रोटी, चावल, दाल।।
हुआ डॉक्टरी देश में, जबसे कारोबार।
घर, खेती तक बिक गये, होने पर बीमार।।
गरिमा जी के दोहों में सामान्य जनों से ज्यों-ज्यों निकटता बढ़ती है वैसे ही संवेदना की बनावट भी स्पष्ट होती जाती है। इसमें कभी संसार और समय की भयावहता और मूल्यहीनता की फ़िक्र दृष्टिगत होती है तो कभी गाँव के चेहरे-चरित्र और शहर की निर्ममता तथा प्रदूषण की चिंता अभिव्यक्ति पाती है। एक तरफ़ गरिमा जी जहाँ नीतिशून्य, कला विहीन, संवेदनहीन जीवन पद्धति का हिस्सा होते जा रहे इस मानव समाज को दर्पण दिखाती हैं वहीं प्राकृतिक बदलावों से मानव के अस्तित्व पर जो ख़तरा उत्पन्न होने वाला है उसके लिये सावधान भी करती हैं। यथा-
झुलसा आँगन रो रहा, कोस रहा है भाग।
माना जिसे चिराग़ था, लगा गया वह आग।।
ज़हर, कोख, जीवन, धरम, देह, अंग-व्यापार।
जाने किस-किस चीज़ को, बेच रहा बाज़ार।।
कमरे जैसा घर हुआ, बालकनी: उद्यान।
ऐसे में खोजें कहाँ, आँगन औ दालान।।
सूखे कोयल का गला, कैसे गाये गान।
दूर-दूर तक जल नहीं, दिखते सिर्फ़ मकान।।
स्त्री, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। ईश्वर ने इन्हें वह छठी इन्द्रिय प्रदान की है जिससे वह दृष्टि, स्पर्श और भाव के विभेद को आसानी से पढ़ लेतीं हैं। वह जितनी सहनशील होती हैं, मानसिक रूप से उतनी सबल भी। स्त्री अपने स्त्रीत्व की संकुचित सीमा में रहकर लज्जा का सम्मान भी करती है और इस संकुचन को त्यागकर प्रेम और मातृत्व की सुधा भी बरसाती है। लेकिन उसकी यही सहनशीलता उसे हमेशा से कमज़ोर भी बनाती रही है। दुनिया का एकमात्र देश भारत जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ उसके साथ दुर्व्यवहार भी कम नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में गरिमा जी जहाँ नारी के महत्व को अंकित करती हैं, वहीं उसके साथ होने वाले अत्याचार का विरोध भी। यथा-
कठिन परिस्थिति में सदा, लेती ख़ुद को ढाल।
नारी इक बहती नदी, जीवन करे निहाल।।
तार-तार होती रही, फिर भी बनी सितार।
नारी ने हर पीर सह, बाँटा केवल प्यार।।
मन के जख़्मों की कहो, कहाँ लगाऊँ हाँक।
पत्नी ने यह सोचकर, लिया चोट को ढाँक।।
पहनावा ही था ग़लत, किया सभी ने सिद्ध।
चिड़िया रोती रह गई, बरी हो गये गिद्ध।।
गरिमा जी जहाँ एक तरफ समाज को उसका वीभत्स रूप दिखतीं हैं, वहीं समाधान-पथ दिखतीं और ढाढस देती भी नजर आती हैं। यथा-
ओ नारी! सुन तू नहीं, एक उतारा वस्त्र।
पा ले हर अधिकार को, उठा स्वयं अब अस्त्र।।
बेटी के अधिकार में, आये क़लम-दवात।
इससे अच्छी है नहीं, बेटी को सौगात।।
वृक्ष लगाना मान लो, सबसे सुंदर काज।
तभी सुरक्षित कल यहाँ, जब सुधरेगा आज।।
चाहे कुहरे ने किये, लाखों कठिन सवाल।
पर सूरज के हाथ में, जलती रही मशाल।।
आज दोहा हिन्दी छंदों में सर्वाधिक लिखा जाने वाला छंद है। दोहों का उत्पादन इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि उसमें मौलिकता की भारी कमी देखने को मिलती है। वैसे भी कविता का सौंदर्यबोध चाहे वह शिल्पात्मक हो या भावनात्मक, तभी तक उसमें श्रोता या पाठक डूब पाते हैं जबतक वह विविधता और सही संप्रेषणीयता को बनाये रखता है।
जैसे ही संप्रेषण की समस्या खड़ी होती है, कविता बहुत पीछे छूट जाती है और मात्र शब्द-विन्यास ही शेष रह जाता है। ऐसे में अनकहे विषय को चुनना और उसपर लिखना एक विशेष कार्य सिद्ध हो सकता है। गरिमा जी के डाॅल्फिन जैसे आवश्यक मगर उपेक्षित विषय पर लेखन इस संग्रह को इसी प्रकार विशिष्टता प्रदान करता है-
डॉल्फिन अपने नृत्य से, भरती मन में प्यार।
उछल-कूद करतब करे, करती जल-बौछार।।
डॉल्फिन है जल की परी, यह गंगा की गाय।
इसे बचाने के लिए, सब मिल करें उपाय।।
गंगा की है गाय यह, सूँस गंग जल रत्न।
इसे बचाने को पुनः, हो अशोक सम् यत्न।।
इस संग्रह के दोहों में जहाँ तत्सम, उर्दू, अंग्रेजी और अन्य देशज शब्दों के प्रयोग इन्हें भाषायी विविधता प्रदान करते हैं वहीं सटीक और नव्य उपमान विधान, प्रतीक, बिम्ब, ऐतिहासिक चरित्र तथा कथाओं से लिये गये पात्र उन्हें कलात्मकता और तीक्ष्ण सम्प्रेषणीयता प्रदान करती है। यथा-
किसी श्वेत खरगोश-सी, उग आई है भोर।
चीर रहा है कोह को, यह किरणों का शोर।।
ठहरी इक पल, फिर खिली, हामिद की मुस्कान।
छोड़ खिलौना ले लिया, चिमटा अच्छा जान।।
मुझे कभी भाया नहीं, इत्रों का बाज़ार।
मैं ख़ुद में जीती रही, बनकर हरसिंगार।।
मोबाइल में हैं बिजी, घर के सारे लोग।
अम्मा बैठी सोचती, लगा बेतुका रोग।।
धूप उजाला माँगती, जा दीपक के पास।
‘गरिमा’ कितना क्षीण अब, हुआ आत्मविश्वास।।
गरिमा जी ने दोहा के पारंपरिक रूप अर्थात नीति और श्रृंगार पर भी पर्याप्त दोहे कहे हैं-
जिन वृक्षों की पत्तियाँ, झड़कर बनतीं खाद।
उनके नव-वंशज सदा, रहते हैं आबाद।।
कुल्हाड़ी औ बाँसुरी, लकड़ी के अनुवाद।
तुम पर है जो बाँट लो, नफ़रत या आह्लाद।।
हार गया वरदान तब, जीत गया प्रभु-जाप।
जली होलिका थी कहाँ, जला अहम् औ पाप।।
जहाँ प्रेम होता सघन, सच्चा और अनूप।
एक दूसरे में वहाँ, दिखता प्रिय-प्रतिरूप।।
जब से इस मन में जगे, प्रेम भरे जज़्बात।
सिंदूरी-सा दिन हुआ, हुई दूधिया रात।।
गरिमा जी को संग्रह के कुछ दोहों के चयन में सावधानी रखने की आवश्यकता थी। कुछ दोहों में भाव और भाषा बेहतर तरीके से संप्रेषित हो सकते थे। समय और अनुभव के साथ नये दोहों में प्रौढ़ता अवश्य आयेगी। एक बेहतरीन संकलन के लिये हार्दिक बधाई।